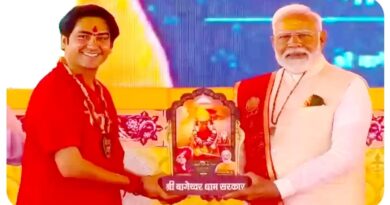आत्मा को विद्युत प्रवाह (बिजली) माने तो उसी से प्रकाशित “बल्ब” शरीर के सामान है
शरीर
सनातन धर्म (हिन्दू धर्म) में वर्णन है कि संसार से बंधी हुई आत्मा, “मृत्यु लोक”, (अर्थात ब्रह्माण का वो जगत जहाँ जीवन मौजूद है), में जन्म लेती है। इसी लोक में वो जन्म, जीवन और मृत्यु का आभास करती है, इसलिए इस लोक को “मृत्यु लोक” या मौत अथवा विनाश का लोक कहा जाता है। शरीर वो महत्वपूर्ण श्रेणी है जिसके द्वारा आत्मा अपने आप को प्रत्यक्ष (जीवित) रूप में ज़ाहिर करती है। अगर आत्मा को विधुत प्रवाह (बिजली) माने तो उसी से प्रकाशित “बल्ब” शरीर के सामान है। ‘शरीर’ संस्कृत भाषा का शब्द है जो देह या काया या भौतिक स्वयं को संबोधित करता है। वेदांत में ”तीन शरीर के सिद्धांत” के अनुसार मनुष्य के तीन शरीर या तीन देह होती है:
– कारण शरीर
– सूक्ष्म शरीर
– स्थूल शरीर
कारण शरीर को जानने से पहले, आइए आत्मा पर एक नज़र डालते है। वह सच्चिदानन्द है या सत्-चित्-आनंद है।

* आत्मा, सत् के रूप में (संस्कृत जड़ से, होना) : सत् वो है जिसका अस्तित्त्व है, सत् उस मूलतत्त्व को संबोधित करता है जो पवित्र है और काल से परे है, जो अपरिवर्तनीय है। यह जन्म से पहले, जीवन काल में तथा मृत्यु के उपरांत अर्थात काल की तीनो अवस्था में एक सामान विद्यमान है। सभी जीवित प्राणी जन्म से पूर्व और मृत्यु के उपरांत उपस्थित नहीं होते, वो मात्र जन्म से मृत्यु काल के मध्य ही अस्तित्व में होते है। परन्तु सत् कालचक्र से परे, सर्वदा विद्यमान है।
न जायते म्रियते वा विपश्चिन्
नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् ।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ कठ उपनिषद् १.२.१८ ॥
आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना ही मृत्यु को प्राप्त होती है। यह न तो किसी में से पैदा हुई है, ना ही इसमें से कुछ पैदा हुआ है। अजन्मी, सनातन, चिरस्थायी, अन्नत, पौराणिक, यह आत्मा शरीर के मरने पर मरती नहीं है। ~ कठ उपनिषद्- १.२.१८

* आत्मा चित् के रूप में : जिसे अपनी वृद्धि या अपने आप को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता ना हो, उसे चित् कहते है। चित् स्वं- प्रकाशमान है। उदहारण के तौर पे, सूरज को देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं के प्रकाश से ही प्रकाशमान है।
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ कठ उपनिषद् २.२.१५ ॥
सूरज, चाँद, तारे, बिजली और आग का प्रकाश उस रौशनी के सामने नहीं चमक सकता। उसकी चमक सर्वोत्तम है, शेष समस्त उसी के प्रकाश से प्रकाशमान है। वह प्रकाश अलौकिक है। ~ कठ उपनिषद्- २,२,१५ ; मुकुंद उपनिषद् – २,२,१० ; शेतसार उपनिषद्- ६,१०
* आत्मा आनंद के रूप में : आत्मा जो की अनंत और सनातन है, जो स्वं- प्रकाशमान है, वो परम आनंद की तरह है। ” विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” : ब्रह्म विज्ञान है, परम आमोद है। ~बृहदारण्यक उपनिषद् – ३, ९, २८
” आनन्दं ब्रह्मेति व्यजानात”: ऋषियों ने कहा है आनंद ब्रह्म है। ~तैत्तिरीय उपनिषद् ३, ६
“प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति “: प्राण ब्रह्म है, जो आनंद (कं) है, वही आकाश (खं) है, वो भी ब्रह्म है। ~छान्दोग्य उपनिषद् – ४, १०, ५
“स एष प्राण एव , प्रज्ञात्मा अनन्दःजरोःमृत” : वो ही प्राण है, वो ही प्रज्ञा है, वही आनंद है जो अजय-अमर है। ~कौषीतकि उपनिषद्- ३,८
यह आनंद साधारण प्रसन्ता नहीं है, ये परम चिरस्थायी आनंद है। “एत् सैयव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मत्रमुपजिवन्ति “- इस आनंद के कणों पर सभी जीव जीवंत है। ~ बृहदारण्यक उपनिषद्- ४,३,३२
☛ कारण शरीर : हिन्दू धर्म में कारण शरीर को मुख्यतय आत्मा या सच्चिदानन्द से संग्लित बताया गया है। आत्मा के कारण शरीर का विवरण हिन्दू धर्म से पहले किसी भी अन्य धर्म में नहीं किया गया है। कारण शरीर ही संसार से बंधी हुई आत्मा या वो आत्मा ओ कारण शरीर से आसक्त हो के अगले जन्म में उसके स्थूल और सूक्ष्म शरीर का एकमात्र कारण है। कारण शरीर पिछले जन्म में अर्जित समस्त ज्ञान और जानकारी को बीज रूप में संजोता है। सांसारिक सुखों के प्रति गहन आसक्ति या “वासना” इसके साथ ही जाती है। आत्मा कारण शरीर से बड़ी दृढ़ता से बंधी हुई है।
कारण शरीर प्राथमिक रूप से माया का बना हुआ है, इसी वजह से उसमे माया के सभी गुण है। इसके निम्न गुण उल्लेखनीय है: अनादी (जिसका प्रारंभ और अंत न हो), अविद्या (अज्ञान) तथा अनिर्वाचा (अकथनीय या जिसका वर्णन न किया जा सके)। मरने के बाद स्थूल और सूक्ष्म शरीर राख हो जाते है या प्रकर्ति में विलीन हो जाते है। परन्तु कारण शरीर मायान्वित (या माया से ग्रस्त) आत्मा के साथ ही जाता है, जहाँ भी वो जाये, जब तक की वो सम्पूर्ण रूप से मुक्त न हो। जैसे ही आत्मा माया से बने इस कारण शरीर से मुक्ति पा लेती है, वो ब्रह्म की अवस्था में विलीन हो जाती है। हिन्दू धर्म में आत्मा की इस मुक्ति को “अत्यानिक मोक्ष” या सम्पूर्ण मुक्ति कहा गया है।
इसका अभिप्राय जन्म और मृत्यु के चक्र या संसार चक्र से मुक्ति से भी है क्योंकि इसके उपरांत आत्मा को फिर कभी मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता यदि इश्वर की भी यही इच्छा हो तो।
कारण शरीर “चित्त” द्वारा बनाया हुआ है। अविद्या का कण “अणु ” सार्वलौकिक प्रेम, चित्, के प्रभाव से आध्यात्मिक रूप ले लेता है, जैसे की चुम्बकीय शेत्र में रखने पर लोहा चुम्बकत्व ग्रहण करता है, और चेतना (अनुभूति की शक्ति) द्वारा संसाधित करने पर, इसे चित्त, मन या दिल कहा जाता है। इसमें ही स्वयं के अलग होने का आभास होता है, जिसे अहम्कार कहा जाता है। इस प्रकार चुम्बकत्व ग्रहण करने से मन के दो ध्रुव बन जाते है। एक सकारात्मक जिसे ”बुद्धि” कहा जाता है और दूसरा नकारात्मक जिसे ”मानस’ कहा जाता है। बुद्धि का स्वाभाविक झुकाव सत् की ओर है, और मानस माया से आकर्षित है।__________________
स्थूल शरीर अन्नमय कोष, सुष्म शरीर प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, तथा कारण शरीर आनंदमय कोष है। कारण शरीर ही सुष्म शरीर और स्थूल शरीर का जनक या कारण है।
-साभार।