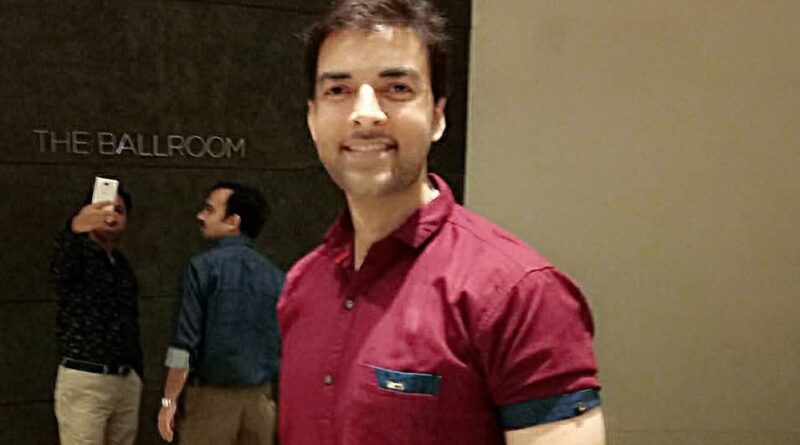देवेंद्र सिकरवार : नागों का रहस्य.. अग्रवालों, कायस्थों, टांक राजपूतों और कालबेलिया जातियों में.. परंपरा, इतिहास और एक विलुप्त संस्कृति की जीवित स्मृति
-क्या आपने सोचा है कि अग्रवालों, कायस्थों, टांक राजपूतों और कालबेलिया जातियों में क्या समानता है?
-क्या आपने सोचा है कि मकान की नींव बनाते समय सोने, चांदी या ताँबे का नाग क्यों दबाया जाता है।
-क्या आपने सोचा है कि हमारे समाज में ‘नाग पंचमी’ और ‘अनंत चतुर्दशी’ क्यों मनाई जाती है?
क्या इनका आधार सिर्फ धार्मिक है या सुदूर अतीत की किसी ऐतिहासिक स्मृति को बनाये रखने का प्रयत्न है?
वस्तुतः इस प्रश्न का उत्तर मनोविज्ञान के एक प्रश्न में ही निहित है।
“मानव साँपों से इतना डरते क्यों हैं?”

इसके उत्तर में एक ‘जेनेटिक हाइपोथीसिस’ रखी गई जिसके अनुसार-
“डायनासौरों के युग में मानव के आदिपूर्वज श्रूज जैसे छोटे स्तनियों के रूप में थे और स्पष्टतः उनकी स्थिति डायनासौरों के समक्ष संकटपूर्ण थी। इसीलिये डायनासौरों के प्रति वह भय उनकी जीन संरचना में समाहित हो गया। कालांतर में बड़े डायनासौर विलुप्त हो गए और उनकी कुछ छोटी सहप्रजातियों के वंशज सांपों में विकसित हो गए।
आगे चलकर विकास की दौड़ में पहले स्तनी आगे निकले और फिर उन सबमें मनुष्य।
मनुष्य भले ही इस ग्रह का सर्वाधिक शक्तिशाली जीव बन गया लेकिन उसकी जीन संरचना में सरीसृपों के प्रति धंसा हुआ भय जस का तस बना रहा और मनोविज्ञान के अनुसार जिसके प्रति भय होता है उसके प्रति मनुष्य का व्यवहार दो अतिरेकी ध्रुवों से संचालित होता है — वह या तो भय के कारक को मार डालता है या फिर उसकी पूजा करता है।”
साँपों के प्रति मानव का यह द्वैध व्यवहार विश्वव्यापी है।
एक ओर उसे देखते ही मनुष्य के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह उसे मार डालने हेतु तत्पर हो उठता है वहीं दूसरी ओर विश्व में एक भी प्राचीन सभ्यता ऐसी नहीं जिसमें साँपों को पूजा न गया हो।
इसीलिये प्रागैतिहासिक युग में जब मनुष्य में मानव के जन्म, उसकी मृत्यु, मृत्यु के बाद जीवन परलोक आदि मान्यताओं के रूप में ‘धर्म’ का विकास हो रहा था, तब उसके इस भय के परिणाम स्वरूप उदय हुआ ‘टोटम’ का।
टोटम!
एक ऐसा जीव या पदार्थ जिससे कोई कबीला स्वयं की उत्पत्ति भी मानता है और उसके प्रतीक चिन्ह की पूजा भी करता है।
आज भी हर हिंदू जाति के कुलपशु, कुलपक्षी, कुलवृक्ष के रूप में यह टोटम प्रथा उपस्थित है।
भारत के हिमालय क्षेत्र में भी एक टोटम जाति का विकास हुआ और चूँकि पहाड़ों को संस्कृत में कहते हैं ‘नग’ इसलिए ये कहलाये–
————– ‘नाग’————
‘नाग’ उस आदिम जनजाति के मनुष्य थे जो सर्प से अपनी उत्पत्ति मानते थे और उसके प्रतीकों को अपने गाँवों में गणस्तंभ पर, मुख्य द्वार पर, घरों पर, यहाँ तक कि अपने शरीरों पर चित्रित करते थे।
चूँकि ये कबीले यायावर वृत्ति के थे और संस्कृत में ‘सर्प’ का अर्थ है चलना, अतः ये और इनका टोटम जीव ‘सर्प’ भी कहलाये।
इसी यायावर ‘सर्प’ वृत्ति के कारण यह टोटम जाति कश्मीर से लंका तक तक और सिंध से लेकर पूर्वी भारत तक फैल गई। यहाँ तक कि इनके कुछ कबीले समुद्री रास्तो से पश्चिमी एशिया में मिस्र व पूर्वी एशिया में फिलिपीन्स तक पहुंचे।
इस्लाम पूर्व के मिस्र में और वर्तमान में भारत व चीन में इनके द्वारा प्रसारित नाग पूजा के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं । भारतीय परंपरा में अच्छे और दुष्ट दोंनों प्रकार के नागों का विवरण है और ‘अनंत शेष’ को तो ईश्वर का ही रूप माना गया है।
पूर्वी यूरोप में सर्प ड्रेगन के रूप में भयकारक है जबकि चीन में वह पूज्य है ।
इन उदाहरणों से नाग संस्कृति के वैश्विक प्रभाव का सहज ही अनुमान हो जाता है ।
भारत में मूलतः यह कश्मीर में यह ‘पिशाच’ जाति के साथ रहते थे और जब महारुद्र शिव ने उन्हें परास्त कर दिया तो उन्होंने आर्य संस्कृति की गोत्र प्रथा में ‘कश्यप’ गोत्र को ‘पितृ गोत्र’ के रुप में अपनाया लेकिन मातृ गोत्र ‘कद्रु’ यथावत रहा।
चूँकि इनमें ‘ संस्कृति ‘ का तत्व प्रधान था ना कि नस्ल और रंग का और शायद इसी कारण इनका वैश्विक प्रसार हो सका।
सर्पों के वर्गीकरण के आधार पर इन्होंने अपने कबीलों को भी वही नाम दिये जैसे
-‘अनंत या शेष कबीला जो कश्मीर के अनंतनाग क्षेत्र में निवास करता था और विष्णु के प्रति निष्ठा रखते थे। इनका प्रभाव इतना अधिक बढ़ा कि वे नागों में ही नहीं बल्कि आर्यों में भी ईश्वर के रूप में पूजे जाने लगे कि वह सम्पूर्ण पृथ्वी का वहन करते हैं और इसीलिये उनके प्रतीक के रूप में नींव में धातु का नाग रखा जाने लगा।
-‘वासुकि’ कैलाश क्षेत्र के निवासी थे जिनका महारूद्र शिव से घनिष्ठ संबंध था, यहां तक कि यह कहा जाने लगा कि वासुकि तो शिव के गले के हार हैं। अनंत के बाद इनका प्रभाव नागों पर सर्वाधिक था और वह सभी नाग कबीलों के राजा माने जाते थे।
-‘कर्कोटक’ कबीला भी कश्मीर का ही मूल निवासी था जिसके किसी सदस्य ने राजा नल की सहायता की और आगे जाकर वह कश्मीर को एक महान राजवंश भी देने वाले थे।
‘डिंडिभि’ मैदानी क्षेत्र में विचरण करने वाली शांतिपूर्ण जाति थी।
‘आर्यक’ जाति का संबंध आर्यों से बहुत गहरा था जो उनके नाम से ही स्पष्ट है। यहाँ तक कि उनके यदुओं से विवाह संबंध भी बने और उनका मातृ पक्षी रक्त से कृष्ण का जन्म होने वाला था।
इन सबके बीच नाग जाति का सबसे उद्दंड, परम्परावादी और विषैला कबीला था ‘तक्षक’ जिनमें अपनी दैवी श्रेष्ठता का अहंकार था। वर्तमान दिल्ली से लेकर उड़ीसा तक अर्थात तत्कालीन खांडव वन से लेकर मणिपूर तक इनके सदस्य बिखरे हुये थे। इसी कबीले के कारण भारत में नागों व आर्यों के बीच भयानक संघर्ष प्रारम्भ हुआ।
प्राराम्भिक संघर्षों के बाद सांस्कृतिक रूप से यह जाति मनु के वंशज आर्यों में विलीन हो गयी और अंतिम रूप से गुप्त काल में इनका पृथक अस्तित्व सदैव के लिये समाप्त हो गया परंतु ‘अनंत चतुर्दशी’ , ‘नाग पंचमी’ और ‘पृथ्वी के शेषनाग पर टिके होने’ की परिकल्पना से भारतीय समाज पर इनके प्रभावों का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है ।
आदिकाल से लेकर मुस्लिमों से संघर्ष तक भारत के इतिहास में इन कबीलों ने भिन्न-भिन्न रूपों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।
-नागों ने जलप्रलय में मानव जाति की नेवीगेशन में सहायता की।
-नागों ने ऑपरेशन ‘सागर मंथन’ में देवों व दैत्यों के कम्युनिकेशन में मदद की।
-नागों की निष्ठा महारुद्र शिव के प्रति भी थी और विष्णु के प्रति भी।
-नागों ने आर्यों से शत्रुता भी निभाई और मित्रता भी।
-नागों ने बुद्ध व महावीर के लिए कवच का कार्य भी किया।
-नागों ने कुषाणों का प्रतिरोध किया।
-नागों ने काशी में दशाश्वमेध घाट भी बनाया।
-नागों ने जनमेजय का प्रतिशोध भी झेला और समुद्रगुप्त का कहर भी।
-नागों ने यौधेयों को लड़कियां भी दीं तो ललितादित्य के रक्तपूर्वज भी बने।
-उनका रक्त राजपूतों, जाटों, अग्रवालों व कायस्थों में है तो कालबेलिया व संपेरों में भी।
आज नाग मंदिरों में भी हैं और हम सबके रक्त का हिस्सा भी।
नागपंचमी का त्योहार हिंदुओं की सर्वसमावेशीकरण का प्रतीक भी है और स्वयं में एक इतिहास भी।
क्योंकि पश्चिम ने इतिहास लिखा किताबों में और हमने उसे संजोया परंपराओं व त्योहारों में।
इच्छाधारी नागों के मिथक से इतर और टीवी सीरियलों के ज्ञान से अलग ‘नाग’ ऐसी नृजाति थे जिनके वंशज आज भी हमारे आपके बीच में हैं।
———
‘अनसंग हीरोज : #इंदु_से_सिंधु_तक के अध्याय ‘टोटम युग के यात्री’ का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण।