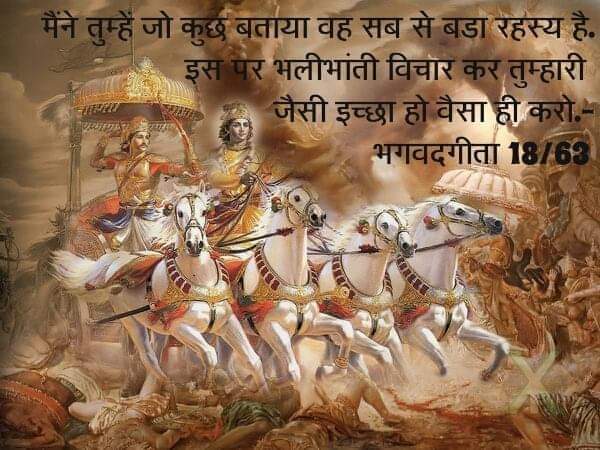विद्यासागर वर्मा : वैदिक मान्यताए.. ईश्वरीय ज्ञान (भाग 32) X) वेदों में विज्ञान (13), वेदों में मनोविज्ञान (1)
( Psychology in the Vedas )
i) मन का स्वरूप
( शंका समाधान )
हमारे इस लेख पर कुछ महानुभावों ने मन तथा जीव सम्बन्धी
कुछ शंकाएं उठाई हैं, जिन का समाधान/स्पष्टीकरण प्रस्तुत है :
क) मन का स्वरूप
i) इस विषय पर हमने जो भी विचार प्रस्तुत किए हैं, हमारे नहीं हैं। वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रन्थों, गीता आदि के विचारों को, उनके उद्धरणों सहित व्याख्यित किया है। गहन विषयों को ऋषियों ने अपने – अपने ढंग से प्रस्तुत किया है, जिन में विरोधाभास ( विरोध का आभास / शक/ appearance ) हो सकता है, विरोध नहीं। Nothing is contradictory in our Scriptures.
ii) केन ( किस के द्वारा ) उपनिषद् (1.2) के ऋषि का कथन है :
“श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाच: स उ प्राणस्य प्राणः। चक्षुषश्चक्षु: —–।।
अर्थात् वह (आत्मा) श्रोत्र की श्रवण शक्ति है, मन की मनन शक्ति, जिह्वा की वाक् शक्ति, प्राण की श्वास-प्रश्वास गति और आँखों की ज्योति/देखने की शक्ति है ।

इसी आशय का ‘ प्रश्न उपनिषद् ‘ का श्लोक (4.9) है :
” एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता ।
मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः ।।”
अर्थात् यही देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूँघने वाला, स्वाद अनुभव करने वाला, मनन करने वाला, बुद्धि से काम करने वाला, कर्ता, ज्ञान प्राप्त करने वाला चेतन स्वरूप आत्मा पुरुष है।
स्पष्टत: यहां आत्मा (Soul) को सभी कार्यों का कर्ता कहा गया है।
iii) शतपथ ब्राह्मण (14.4.3.8) का वाक्य है :
” मनसा ह्येष पश्यति, मनसा श्रृणोति।”
अर्थात् निश्चित रूप में, आत्मा (मनसा) मन के माध्यम से देखता है,
मन से सुनता है।
महाभारत ( शान्तिपर्व 311.17) का कथन है :
” चक्षु: पश्यति रूपाणि मनसा न तु चक्षुषा।”
अर्थात् अर्थात् आंख रूपों को मन से देखती है ,
चर्मचक्षु ( Sense – organ ) से नहीं।
iv) उपरोक्त शास्त्रीय प्रमाणों में विरोधाभास ( विरोध का शक ) तो हो सकता है, परन्तु विरोध है नहीं।
सामान्य जन तो यही जानते हैं कि हम आंखों से देखते हैं। महाभारत ने स्पष्ट कर दिया कि आंख की पुतली नहीं देखती, मन देखता है, मन सुनता है। हमने कई बार महसूस भी किया है कि पास में नगाड़ा बज रहा होता है, परन्तु सुनाई नहीं देता क्योंकि मन उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा होता, किसी और विषय में व्यस्त होता है।
इसी विषय को केन तथा प्रश्न उपनिषद् ने और अधिक स्पष्ट कर दिया कि सुनने वाला आत्मा है, तथा वह ” मनसा ” मन के माध्यम से सुनता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मन केवल यंत्र ( Instrument ) है। आत्मा ही सभी कर्मों का कर्ता और भोक्ता है।
ख) मोक्ष का कारण मन
हमने अपने लेख में दो उद्धरण दिए — एक ब्रह्मबिन्दु उपनिषद् का और दूसरा जाहन मिल्टन का।
‘‘ मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः’’ ।
— ब्रह्मबिन्दु उपनिषद्-2
अर्थात् मन ही जीव के बन्ध (बन्धन, Bondage) या मोक्ष (Salvation/ Liberation) का कारण होता है क्यों कि सभी शुभ व अशुभ कर्म मन के द्वारा किये जाते हैं।
मन अपने स्थान पर और अपने आप,
स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना सकता है।
— जाहन मिल्टन (पैराडाइज़ लास्ट)
i) यहां प्रश्न उठाया गया है कि कर्म का कर्ता और कर्मफल का भोक्ता कौन है ?
हम ने लेख में कहा कि वैदिक मनोविज्ञान में मन जड़ है और आधुनिक मनोविज्ञान में मन चेतन ( Conscious).
स्पष्टतः आधुनिक मनोविज्ञान में कर्ता और भोक्ता मन ही है क्यों कि Psyche ( Spirit/ आत्मा ) को ही Mind / मन मान लिया गया है।
ii) हमने अपने लेख में ब्रह्मबिन्दु उपनिषद् के उद्धरण से मन को मोक्ष का कारण बताया है। स्पष्टतः कारण कर्ता नहीं हो सकता; अतः आत्मा ही कर्ता है और जो कर्ता होता है ,वही भोक्ता होता है।
हमने मन को जड़ अपनी ओर से घोषित नहीं किया। हमारे सभी ग्रन्थों में मन को जड़ कहा गया है क्यों कि यह प्रकृति की उपज ( Product) है। प्रस्तुत है इस संबंध में स्वामी विवेकानन्द की मन की व्याख्या :
” Mind at a very low rate of vibration is what is known as Matter. Matter at the high rate of vibration is what is known as Mind. Both are the same substance.”
अर्थात् न्यूनतम कम्पन वाला मन द्रव्य (Matter) कहा जाता है। कम्पन की अधिक गति वाला द्रव्य मन कहलाता है। दोनों एक ही वस्तु हैं।
ग) मन की चेतना आत्मा की ही चेतना है जैसे सूर्य के प्रकाश से चन्द्र प्रकाशित हो जाता है। मन के सभी कार्य आत्मा से ही प्रेरित होते हैं।
i) इस विषय पर प्रश्न उठाया गया है कि आत्मा मन को अकल्याणकारी संकल्पों में क्यों धकेलता है ?
आत्मा द्वारा जन्म-जन्मांतर में किए गए शुभ – अशुभ कर्मों के संस्कार सूक्ष्म शरीर में संग्रहीत रहते हैं, ये वासना के रूप में मन में , जो सूक्ष्म शरीर का अंग है, उभरते रहते हैं। ये आत्मा की ही दबी हुई इच्छाऐं हैं जो मन में संकल्प रूप में अभिव्यक्त होती रहती हैं। इसी प्रकार शुभ कर्मों के संस्कार शुभ संकल्पों को उभारते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहता है परन्तु छोड़ नहीं पाता। मनुष्य को पता होता है कि उसे धर्म कार्य करने चाहिये परन्तु करने में उसकी रुचि नहीं होती। इस स्थिति को महाभारत में दुर्योधन के मुख से इस प्रकार व्यक्त किया गया है :
” जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति
जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्ति ।
केनापि देवेन हृदिस्थितेन
यथा नियुक्तोsस्मि तथा करोमि ।।”
अर्थात् मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है परन्तु मेरी इसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं जानता हूँ कि अधर्म क्या है परन्तु मेरी इस से निवृत्ति नहीं होती। मानो हृदय में बैठे किसी देवता से मुझे जैसा आदेश होता है, वैसा करता हूँ।
यह देवता और कोई नहीं, अपने पूर्व कर्मों से सिंचित वासना एवं सस्कार हैं, स्वभाव है।
ii) प्रश्न यह भी उठाया गया है कि जब मन कुछ करता ही नहीं ” तन्मे मन: शिवसंकल्पमस्तु ” की प्रार्थना का क्या औचित्य है ?
प्रार्थना ईश्वर से की गई है मन से नहीं। क्या हम ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे ?
प्रार्थना से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं ” धियो यो न प्रचोदयात् “: हे प्रभो ! हमारी बुद्धि को शुभ कर्मों में प्रेरित करो, तो हमारे मन में भाव जगते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और हम उस दिशा में प्रयत्न भी करते हैं। ऐसा करने पर हमारे पूर्वकृत अशुभ कर्मों की वासनाओं पर भी उभरने से अंकुश लग जाता है। वासनाएं तभी उभरती हैं जब कोई उद्बोधक (Precipitating Cause) हो। गीता (2.62) में कहा गया है ” ध्यायतो विषयान्पुंस: संङ्गस्तेषूपजायते।” अर्थात् जब मनुष्य विषयों के बारे में सोचता है, उसकी विषयों में आसक्ति हो जाती है। तभी मन में विचार/संकल्प भी वैसे उभरने लगते हैं। जब मनुष्य प्रार्थना में, शुभ कार्यों में व्यस्त होगा, वह विषयों के बारे में सोचेगा ही नहीं, अकल्याणकारी संकल्प उठेंगे ही नहीं।
घ) प्रश्न उठाया गया है, जीव क्या है ? मोक्ष का प्रयत्न कौन करता है ?
वैदिक दर्शन के अनुसार तीन सत्ताएं अनादि हैं : ईश्वर, जीव और प्रकृति। आत्मा शब्द वेदों , उपनिषदों में जीव ( Soul) के लिए तथा ईश्वर (God) दोनों के लिए प्रयुक्त किया गया है। भ्रमनिवारण हेतु, जीव को जीवात्मा और ईश्वर को परमात्मा कहा जाता है।
आत्मा परमात्मारूप नहीं है। दोनों भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं। आत्मा की बजाय जीव शब्द अधिक प्रयोग में लाया जाता है ताकि कोई भ्रम ( confusion) न हो। दूसरा, अद्वैतवादी आत्मा शब्द का अर्थ सदा ब्रह्म ही करते हैं। आत्मा/ जीव कर्म बंधन और जन्म – मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, जब तक मोक्ष प्राप्त न कर ले। ईश्वर/ परमात्मा आनन्द स्वरूप है, जीव के कर्मफल का दाता और मोक्ष का प्रदाता है।
मोक्ष के लिए प्रयत्न जीव / आत्मा करता है, मन नहीं।
ब्रह्मसूत्र/ वेदान्त दर्शन का सूत्र है ” आनन्दमयो sभ्यासात् ” अर्थात् जीव अभ्यास से, योग-साधना से आनन्दमय हो सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है।
ङ) मन आत्मा का उपकरण (Instrument) है।
आत्मा बिना शरीर के कार्य नहीं कर सकता। इसका यह अर्थ लेना उपयुक्त नहीं कि कार्य मन ही कर्ता है। सूक्ष्म शरीर तथा मन में जीव के सभी जन्मों के कर्मों का हिसाब रहता है। यह एक पटवारी ( लेखापाल) कि तरह है जो सभी भूखण्डों का लेखा जोखा रखता है। लेखापाल उन भूखण्डों का स्वामी नहीं होता, स्वामित्व सरकार का होता है और उसके पास ही राजस्व जाता है। इसी प्रकार आत्मा/ जीव सभी कर्मों का कर्ता और भोक्ता होता है।
च) मन आत्मा के कर्मों का उत्तरदायी नहीं। रोबोट का उदाहरण।
मानो एक पाकिस्तानी जासूस भारत में ड्रोन ( Drone) के द्वारा हथियार या मादक पदार्थ फैंकवाता है। क्या यहां कर्ता ड्रोन होगा या जासूस ? क्या पाकिस्तान सरकार सफल कार्य के लिए ड्रोन को सम्मानित करेगी या उस जासूस को ?
छ) पिता – पुरुष का आख्यान ( Analogy)
हमने लेख में कहा कि कर्ता तो जीव है, परन्तु दिखाई ऐसे देता है जैसे कि मन ही कर्ता है, और कहा :
” जैसे पुत्र पिता के घर को, अपना ही घर कहता है,
वैसे जीवकृत कर्म को मन, आत्मकृत समझ लेता है।।”
वस्तुत: यह आत्मा और शरीर ( मन/ बुद्धि ) का तादात्म्य ( आत्मभाव) ही मिथ्याज्ञान है, जो दु:ख का कारण है, जीव के बन्धन का कारण है।
……………..
ईश्वरीय ज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु,
कृपया इस पोस्ट को शेयर करें।
…………….
शुभकामनाएं
विद्यासागर वर्मा
पूर्व राजदूत
……………..