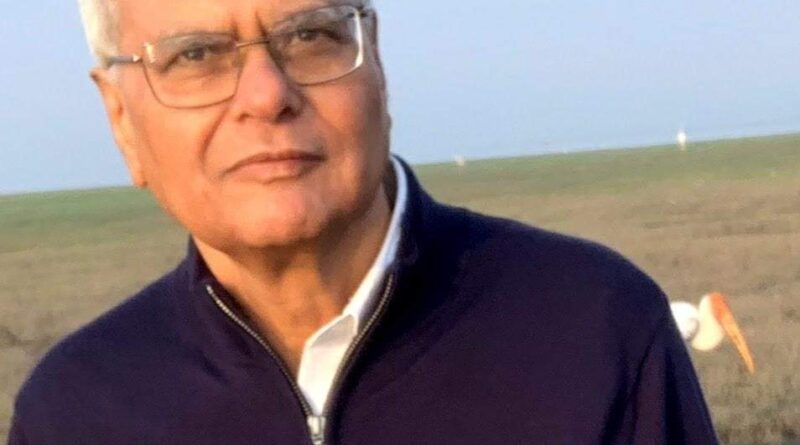कमलकांत त्रिपाठी : याद हो कि न याद हो: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बनाम इतिहास की वर्गनिरपेक्ष तथ्यात्मकता, वर्णव्यवस्था की उत्पत्ति और संस्कृत भाषा की बहुआयामी उपलब्धियां
मुझे वह दिन नहीं भूलता जब अमेरिका में एक ट्रेनिंग कोर्स के दौरान मित्र बने एक पाकिस्तानी सज्जन से बात करते समय संस्कृत भाषा का प्रसंग आया, तो उन्होंने इसके प्रति अतिरिक्त सम्मान दिखाते हुए इसे लैटिन और ग्रीक के समकक्ष कहा. उन्होंने मेरे ही सामने अपने दूसरे पाकिस्तानी साथी को संस्कृत के बारे में कुछ अहम जानकारी देते हुए इसकी बहुत तारीफ़ की. उनके परिवार के बुज़ुर्ग बँटवारे के समय लखनऊ से पाकिस्तान गये थे. वे संस्कृत नहीं पढ़े थे, उन्हें तो देवनागरी लिपि तक नहीं आती थी, उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से ही इसके बारे में सुन रखा था.

इधर अपने देश में संस्कृत को रूढ़िवादी और पुरातनपंथी ही नहीं, शोषण-मूलक ब्राह्मण या सनातन धर्म और अन्यायपूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था का पर्याय मानकर इसे प्राय: दुत्कार दिया जाता है. प्रयोग की बात तो दूर, किसी ने इसका ज़िक्र तक कर दिया तो वह प्रतिक्रियावादी, वर्णाश्रमी, दलित-विरोधी, प्रगति-विरोधी और शोषक वगैरह हो गया. समझ में नहीं आता, सिर्फ़ संप्रेषण के लिए इस्तेमाल होनेवाली भाषा अपने-आप में शोषक कैसे हो सकती है ! भाषा में क्या लिखा जाता है, इस पर भाषा का क्या नियंत्रण ?
जिस काल में संस्कृत का प्रचलन था, स्वाभाविक है कि उसी काल की मान्यताओं, मूल्यों को इसमें अभिव्यक्ति मिली. इतिहास जो भी हो, उसे मिटाया नहीं जा सकता. उससे आँख चुराना सत्य से आँख चुराना है. इतिहास की उपेक्षा चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने में बाधक हो जाती है.
मान्यताओं और मूल्यों के मामले में उस समय विश्व के अन्य हिस्सों में भी कोई बेहतर स्थिति नहीं थी. प्राचीन यूनान में दासों को न केवल नागरिक नहीं माना जाता था, उन्हें मनुष्य की श्रेणी में ही नहीं गिना जाता था, न उनके ऊपर कोई विचार होता था.! अरस्तू ने उन्हें ‘जीवित औजार’ कहकर टाल दिया था. हिंदुओं की ही तरह पुराने यूनानी (और रोमन भी) अनेक देवी-देवताओं की पूजा करते थे और उन्हें ख़ुश करने में लगे रहते थे. उनके भी कई देवता हमारे देवताओं की ही तरह एक से एक विचित्रताओं के पुंज थे.

रोमन साम्राज्य में तो दासों को ग्लेटिएटर के रूप में एम्फ़ीथियेटर में मरने-मारनेवाले द्वंद्व-युद्ध के लिए तैयार किया जाता था, जिसका क्रूर ‘खेल’ संभ्रांत नागरिकों के मनोरंजन का मुख्य साधन था. हावर्ड फ़ास्ट के प्रसिद्ध उपन्यास स्पार्टकस में वर्णित रोमन दासों की हृदय-विदारक स्थिति की ऐतिहासिक प्रामाणिकता संदेह से परे है. लैटिन भाषा की कृतियों में इस दास-व्यवस्था के विरुद्ध कुछ नहीं मिलता, बल्कि सिसरो-जैसे विचारकों ने तो इसे दासों के लिए भी उपयोगी और फ़ायदेमंद क़रार दिया है.
लेकिन ग्रीक और लैटिन भाषाएँ आज भी पढ़ी जाती हैं— अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए और आधुनिक यूरोपीय भाषाओं के भाषाशास्त्रीय विवेचन के लिए. उनका अध्ययन-मनन हेय नहीं माना जाता, जैसे संस्कृत के साथ हमारे प्रगतिशील तबकों में अमूमन होता है. लगता है जैसे प्रगतिशीलों में आत्म-विश्वास की कमी हो– कहीं से कोई झोंका आया नहीं कि उनकी प्रगतिशीलता भहरा पड़ेगी.
पश्चिम में दासों की यह स्थिति बहुत बाद तक बनी रही. अमेरिकी स्वातंत्र्य युद्ध (1775-83) के बाद दक्षिणी राज्यों में वनाच्छादित विशाल भूभाग को साफ़कर कृषि-योग्य बनाना और खेती का तमाम श्रमसाध्य कार्य, अफ़्रीका से घेर-घारकर पकड़े गए और बेहद निर्मम तरीक़े से जहाजों में भरकर अमेरिका लाकर बेचे गए अश्वेत दासों द्वारा ही किया जाता रहा. हैरियेट बीचर स्टोव की अमर कृति Tom Uncle’s Cabin अमेरिकी दासों की दुर्दशा का एक अविस्मरणीय दस्तावेज़ है, जिसने अमेरिकी गृह-युद्ध (1861-65) और उसमें उत्तरी राज्यों की विजय के साथ दास-प्रथा के उन्मूलन को जबर्दस्त प्रेरणा प्रदान की थी—युद्ध के दौरान जब लिंकन इसकी लेखिका से मिले तो बोल उठे—“So, this is the little lady who started this great war.”
यूरोप में यही दास सामंती युग में भू-दास (serf) बन गए, जिनकी स्थिति बँधुआ मज़दूरों-जैसी या उनसे भी ज़्यादा दयनीय थी, वे और उनके वारिस (बिना किसी क़र्ज़ के) जागीर से ऐसे बँधे होते थे कि उसे छोड़कर किसी अन्य जागीर पर नहीं जा सकते थे, जागीरदार जैसा भी हो. औद्योगिक क्रांति के बाद यही भू-दास गाँवों की जागीरों से भागकर कारख़ानों में मज़दूरी करने आ गए. इन मज़दूरों की हालत ऐसी गई-गुज़री थी कि इन्हें मार्क्सवाद में सर्वहारा (proletariat) कहा गया , वे जिनके पास शरीर के अलावा और कोई सम्पत्ति नहीं थी और पूँजीपति द्वारा निर्धारित मूल्य पर श्रम बेचने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था. और उन दिनों यह मूल्य इतना कम होता था कि मज़दूर किसी तरह अपने और अपने परिवार को बस ज़िंदा भर रख सके, ताकि ख़ुद श्रम बेचने के क़ाबिल बना रहे और उसकी अगली पीढ़ी भी इसके लिए उपलब्ध रहे. लेकिन इस सर्वहारा की स्थिति भू-दासों से बेहतर थी क्योंकि सर्वहारा अपने अर्जित वेतन को मन-माफ़िक ख़र्च कर सकता था और कहीं भी जाकर किसी भी कारख़ाने में काम कर सकता था, जो सुविधा भू-दासों को नहीं थी. यही कारण है कि औद्योगिक क्रांति में सबसे आगे रहनेवाले इंग्लैंड के कई ग्रामीण निर्वाचन-क्षेत्रों में इतने कम मतदाता रह गये थे कि उन्हें पॉकेटबरो या रॉटेनबरो कहा जाने लगा था, जहां के सारे के सारे मत आसानी से ख़रीदे जा सकते थे और पैसा ख़र्च करने को तैयार प्रत्याशी के लिए बहुत ‘सुरक्षित’ क्षेत्र माने जाते थे (तो सभी विकसित जनतांत्रिक देश उन या उनसे भी ख़राब स्थितियों से गुज़र चुके हैं, जिनसे अपना देश गुज़र रहा है). इसी तरह भू-दासों की स्थिति भी दासों से बेहतर रही होगी. इससे यूरोप में उन दिनों दासों की क्या स्थिति थी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है.
भारत में न कभी उस तरह का लॉर्ड और वासल के पिरामिड में बंधा सामंतवाद रहा, न भू-दास प्रथा. ज़मींदार (जिनका अधिकार अँग्रेजों के आने के पहले लगान वसूल करने तक सीमित था), बड़े किसान, छोटे किसान और किसान-मज़दूर के बीच अपेक्षाकृत सह-अस्तित्व बना रहा और खेती के साथ-साथ कुशल कारीगरी पर आधारित दुनिया के सर्वाधिक विकसित हस्त-उद्योग के सहारे जन-जीवन में सामान्यत: ख़ुशहाली रही. भूदास प्रथा या उस जैसी किसी शोषक प्रथा के यहाँ अस्तित्व में आने का कोई प्रमाण नहीं मिलता. फ़ाह्यान और ह्वेनसांग के वर्णनों में प्राय: आम जनता में शांति व ख़ुशहाली का ही दृश्य उभरता है और जाति-प्रथा का वह विषम रूप भी सामने नहीं आता जो मध्यकाल और ब्रिटिश काल में प्रशासनिक अवसरों के सीमित होने पर दृष्टिगत होता है. ख़ासकर ब्रिटिश काल में अवसरों की कमी के साथ-साथ हस्त-उद्योग के क्षरण, खेती पर अतिरिक्त भार और पारंपरिक खेती के जबरन नील और अफीम की व्यापारिक खेती में अंतरण जैसे कारणों से बार-बार पड़नेवाले अकालों से स्थिति बेहद विकराल हो गई. फिर भी हस्त-उद्योग पूरी तरह नष्ट नहीं हुए और औद्योगिक क्रांति-जैसी कोई चीज़ यहाँ सम्पन्न नहीं हुई, कि पश्चिमी अर्थ में सर्वहारा का उदय होता !
लेकिन इस अति-प्राचीन भारतीय समाज में बहुत प्राचीन काल से हस्त-उद्योगों के वंशानुगत हो जाने से जाति-प्रथा के रूप में एक भयानक राक्षस पैदा हो गया और व्यवहार में शुचिता के अतिरिक्त आग्रह ने कुछ ज़रूरी हस्त-उद्योगों में लगे समूहों को अछूत बना दिया. उनकी सामाजिक स्थिति की गिरावट ने उनकी मोलभाव की क्षमता को प्रभावित कर उनकी आर्थिक स्थिति भी नीचे गिरा दी.
मुस्लिम शासन में कुछ अछूत मानी जानेवाली तथा बुनकर जैसी अन्य जातियों का धर्मांतरण ज़रूर हुआ लेकिन इन धर्मांतरित समूहों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. ऐसे में प्राय: युद्ध, राज्य-विस्तार और विद्रोह दबाने में लगे रहनेवाले मुस्लिम शासकों को बहुसंख्यक हिंदू-समाज की अंदरूनी बुराइयों को दूर करने की क्या पड़ी थी ! सामाजिक विषमता का यह कोढ़ लगातार बढ़ता ही गया.
मध्ययुग में ही कुस्तुंतुनिया जैसी व्यापारिक मंडियों पर उस्मानी तुर्कों (Ottoman Turks) का क़ब्ज़ा हो जाने (1453) और उनके द्वारा एशिया-यूरोप के बीच का पुराने रेशम और मसाले के व्यापार का ज़मीनी रास्ता बंद कर दिए जाने से परेशान पश्चिमी देशों द्वारा वैकल्पिक मार्ग खोजने की आतुरता ने यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज कराई. यह इतिहास की युगांतकारी घटना साबित हुई और यूरोप के सम्मुख एशिया के आर्थिक-राजनीतिक पराभव का बीज पड़ा. एशिया और यूरोप के बीच व्यापार में लगे अरब व्यापारियों के ऊंटों के क़ाफ़िले अतीत की वस्तु हो गए. पश्चिमी देशों में भारत से समुद्री व्यापार के लिए परस्पर होड़ लग गई. इसके लिए उनके बीच कई लड़ाइयां लड़ी गईं और विजयी इंग्लैंड ने धीरे-धीरे भारत के लाभप्रद निर्यात पर एकाधिकार क़ायम कर लिया. फिर मुग़ल साम्राज्य के पराभव से उपजे शून्य और राजनीतिक अस्थिरता ने भारत को उसे अपने उपनिवेश में अंतरित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया. भारत के प्रभूत और उत्तम कोटि के हस्त-उत्पादनवाली व्यवस्था टूट गई, विश्व-व्यापार में उसका विशाल हिस्सा सिमट गया और निर्यात-अधिशेष (export surplus) उलट गया.
समुद्री व्यापार से आई जीवंतता और आत्म-विश्वास ने पश्चिम में प्रश्नाकुलता, नई खोजों और वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए ज़मीन तैयार की ,जिसने यूरोपी नवजागरण, धार्मिक सुधार और ज्ञानोदय (Enlightenment) को संभव बनाया. पूरब के साथ समुद्री व्यापार से अर्जित पूँजी के चलते इन आविष्कारों का नये यांत्रिक उत्पादन के लिए उपयोग करने का सुयोग उपस्थित हुआ और औद्योगिक क्रांति सम्पन्न हो सकी. फिर तो उपनिवेशों की उत्पादन-प्रणाली पूरी तरह चौपटकर उन्हें कच्चे माल के उत्पादक और तैयार माल के बाज़ार के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा. पूरब पिछड़ गया और पश्चिम पश्चिम हो गया.
जब स्वतंत्र देशों में जनतंत्र की बयार बह रही थी और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो रही थी, हम ग़ुलाम बन चुके थे. ग़ुलामों पर शासन करनेवालों का सारा ध्यान किसी तरह अपना शासन बनाए रखने पर होता है, उन्हें सामाजिक न्याय या सामाजिक समरसता वगैरह के सुधारों से कोई मतलब नहीं होता, बल्कि वे तो सामाजिक विषमता को ‘बाँटो और राज करो’ के लिए ज़्यादा मुफ़ीद पाते हैं. ऊपर से शासन किसी विजेता का न होकर बाह्य व्यापारी कम्पनी का हो तो उसका सबसे ज़्यादा भयावह असर पड़ता है शासित भूक्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था पर. कम्पनी का केंद्रीय लक्ष्य होता है अधिकतम लाभ कमाना और यदि वह संप्रभु सत्ता भी हस्तगत कर ले तो विजित देश और उसकी जनता को इस लाभ-पिपासा का घृणिततम शिकार होना पड़ता है. यही कारण है कि बाह्य व्यापारिक शासन ने साम्राज्यवाद के एक नए और अधिक भीषण रूप—उपनिवेशवाद–को जन्म दिया. इसमें शासक और उसके देश का भविष्य शासित और उसके देश के भविष्य से सर्वथा विच्छिन्न होने के कारण पुरानी अर्थ-व्यवस्ता को पूरी तरह नेस्तनाबूत करने की हद तक उसका आर्थिक शोषण संभव हुआ. वस्तुत: योरोप में वही देश औद्योगिक क्रांति में अग्रणी रहे जो उपनिवेश बनाने की इस होड़ में विजयी हुए. औद्योगिक क्रांति के अग्रदूत इंग्लैंड में इस क्रांति का काल अठारहवीं शताब्दी का वही चरण है जब ईस्ट इंडिया कम्पनी का भारतीय व्यापार अपने निकृष्टतम शोषक अवतार में दिखाई पड़ता है.
इस तरह एक मिथक बन गया कि विषमता और ज़गहों पर भी भले रही हो लेकिन हमारे यहां जाति-व्यवस्था इतनी चालाकी से गढ़ी गई थी कि वह स्थायी हो गई…. अब इतने विलंब से ही सही, जातियाँ ख़त्म करने का सामाजिक काम जिस तरह विशुद्ध राजनीतिक तरीके से हो रहा है, उसे देखते हुए तो यही लगता है वे स्थायी ही साबित होंगी. जैसे यही कि सारी गड़बड़ियों के लिए बेचारी संस्कृत भाषा जिम्मेदार है.
यह ज़रूर है कि संस्कृत में लिखा गया जो ‘शास्त्र’—श्रुति, स्मृति, ‘इतिहास’, पुराण इत्यादि –है, उसमें अमूमन शोषण-मूलक वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रच्छन्न समर्थन है, कहीं-कहीं गुणगान भी. डॉ. अम्बेडकर ने इन्हें छानकर दिखाया है कि हिंदू धर्म का सार तत्व यही जाति-व्यवस्था है और वह इसी के इर्द-गिर्द बुना गया है. इसी अनुभूति ने अंतत: उन्हें अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अंगीकार करने को प्रेरित किया. लेकिन बौद्ध धर्म कब का प्राचीन भारत की मुख्यधारा का अंग बन चुका था. अस्तु अंबेडकर बौद्ध बनने के बावजूद उस मुख्यधारा से बाहर नहीं गए जिसमें धर्म के मामले में चिंतन-मनन और निरंतर समयानुकूल परिवर्तन और सुधार की पूरी छूट है. एक तरह से कहा जा सकता है कि वे सनातन धर्म की व्यापक धारा से अलग नहीं हुए. चूंकि अपने अध्ययन और अनुभव से उन्होंने पाया था कि सनातन धर्म में जाति-व्यवस्था के उन्मूलन की दिशा में समय-समय पर हुए बड़े से बड़े प्रयास असफल रहे थे, दीर्घ काल तक ऊहापोह में रहने के बाद अंत में उन्हें निराशा की-सी स्थिति में बौद्ध धर्म में जाने का यह बीच का रास्ता चुनना पड़ा था.
मुझे लगता है, सनातन धर्म के मूल प्रतिपाद्य पर, उसके सदियों, बल्कि सहस्राब्दियों से घनीभूत होते आनुषंगिक विक्षेप की, यह एक बड़ी विजय थी. और यह एक ऐसे व्यक्ति की अगुआई में हुई जिसकी सोच की निष्ठा और ईमानदारी पर कहीं से संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है. विडंबना है कि सनातन धर्म के पैरोकार इतने पर भी नहीं चेते, बल्कि उन्हें इसके निहितार्थ का एहसास ही नहीं हुआ और वे अभी भी उसी घनीभूत आनुषंगिक धारा में बहे जा रहे हैं.
लेकिन डॉ. अम्बेडकर ने भी जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म से अविच्छेद्य कहा था, संस्कृत भाषा से नहीं. और यह ठोस सच्चाई है कि संस्कृत भाषा में विभिन्न डिसिप्लिन, विभिन्न विधाओं और विभन्न विषयों पर विपुल शास्त्रेतर सामग्री भरी हुई है. हिंदू या ब्राह्मण धर्म से संस्कृत भाषा की पहचान को एकात्म कर देने पर हम स्वभावत: इस शास्त्रेतर विपुल सामग्री से भी वंचित हो जाते हैं.
संस्कृत भाषा में तो दर्शन की एक सुदीर्घ परंपरा रही है जिसमें ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, इस विषय पर विशद विवेचन हुआ है, जो सदियों तक चलता रहा है. संस्कृत ने कपिल-जैसे दार्शनिक दिए जिन्होंने इस विस्तृत विवेचन (सांख्यसूत्र) के द्वारा यह सिद्ध किया कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है—यह सृष्टि जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष के स्वायत्त संयोग की देन है.
तो संस्कृत भाषा को गर्हणीय पुरातनपंथिता और वर्णाश्रमी शोषण का पर्याय मान लेने के बहुत ख़तरे हैं. यह निहायत संकुचित दृष्टि है जो खाँटी प्रगतिशीलता का पोषण करे या न करे, मानव-ज्ञान की परिधि को सीमित अवश्य करती है.
……….